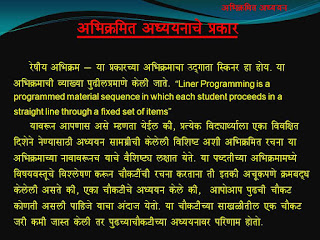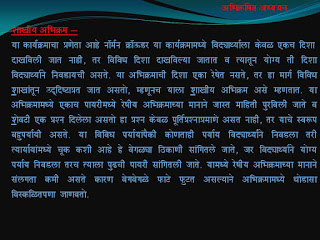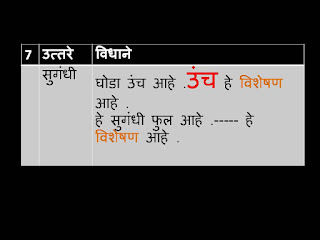About Me

- Dr.Sanjay Shedmake
- H 22 Indraprasth chs near pratiksha nagar bus depot sion, Maharashtra, India
- अन्यायाची चीड यावी असा माझा स्वभाव आहे .मित्र करण्यापेक्षा टिकविणे अधिक आवडते.मी सध्या sndt university,pvdt college of education mumbai येथे प्राध्यापक म्हणून कार्य करतो.
Monday, 24 April 2017
Tuesday, 18 April 2017
संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक आधार: वायगोत्स्की
संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक आधार: वायगोत्स्की की नज़र से
 अमरीका के एक दक्षिणपूर्वी शहर के ट्रैक्टन इलाके में रहने वाले अफ्रीकी-अमरीकी समुदाय के बच्चे कक्षाओं में काफी चुपचाप और सहमे-सिमटे-से रहते थे। शिक्षक बताते कि ये बच्चे सीधे-से-सीधे सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते थे। शिक्षकों और बच्चों के बीच की संवादहीनता का हल ढ़ूँँढ़ने के लिए मानवविज्ञानी शर्ली ब्राइस हीथ ने सुझाया कि ट्रैक्टन समुदाय की भाषा की रीतियों का और शिक्षकों की भाषा की रीतियों का अध्ययन किया जाए। उन्होंने शिक्षकों को अपने खुद के बच्चों के साथ और कक्षा के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए देखा। दोनों ही स्थितियों में शिक्षक बच्चों से बहुत सारे सवाल करते थे। ये ऐसे सवाल थे जिससे यह मालूम चले कि बच्चे कितना जानते हैं, और जिनसे उनके ज्ञान का विस्तार हो। जैसे - “यह किस तरह का ट्रक है?”, “उस तस्वीर में कुत्ते का पिल्ला कहाँ है?” और “यह कहानी किसके बारे में है?”
अमरीका के एक दक्षिणपूर्वी शहर के ट्रैक्टन इलाके में रहने वाले अफ्रीकी-अमरीकी समुदाय के बच्चे कक्षाओं में काफी चुपचाप और सहमे-सिमटे-से रहते थे। शिक्षक बताते कि ये बच्चे सीधे-से-सीधे सवाल का जवाब भी नहीं दे पाते थे। शिक्षकों और बच्चों के बीच की संवादहीनता का हल ढ़ूँँढ़ने के लिए मानवविज्ञानी शर्ली ब्राइस हीथ ने सुझाया कि ट्रैक्टन समुदाय की भाषा की रीतियों का और शिक्षकों की भाषा की रीतियों का अध्ययन किया जाए। उन्होंने शिक्षकों को अपने खुद के बच्चों के साथ और कक्षा के बच्चों के साथ बातचीत करते हुए देखा। दोनों ही स्थितियों में शिक्षक बच्चों से बहुत सारे सवाल करते थे। ये ऐसे सवाल थे जिससे यह मालूम चले कि बच्चे कितना जानते हैं, और जिनसे उनके ज्ञान का विस्तार हो। जैसे - “यह किस तरह का ट्रक है?”, “उस तस्वीर में कुत्ते का पिल्ला कहाँ है?” और “यह कहानी किसके बारे में है?”
इसके विपरीत ट्रैक्टन इलाके में माँ-बाप या अन्य वयस्क बहुत छोटे बच्चों से बिरले ही सवाल करते थे। यहाँ वयस्क बच्चों से तब तक सवाल नहीं करते थे जब तक वे बच्चों को बातचीत करने में परिपक्व और सूचना के स्रोत की तरह न मानने लगें। अगर वयस्क बच्चों से सवाल पूछते भी तो वे ‘सिखाने’ के लिए सवाल नहीं पूछते थे, वे असली चीज़ों के बारे में सवाल पूछते थे। ऐसे सवाल जिनका उत्तर उन्हें भी मालूम न हो और जिस सवाल का कोई एकमात्र ‘सही जवाब’ न हो। जैसे - “वो किसके जैसी है?” या “आज सुबह मिस सैली को सुना क्या?” ये ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर विस्तारपूर्वक देने पड़ते, जहाँ सिर्फ एक सही या गलत जवाब नहीं होता। घर पर ये बच्चे बड़ी कुशलता से बातचीत करते थे - कहानी कहते और हाज़िरजवाब होते - पर यह योग्यता स्कूल में उनके काम नहीं आती। स्कूल में पूछे गए सवालों से ये बच्चे चकरा जाते और चुप्पी साध लेते।
जब हीथ ने शिक्षकों से इस तरह के उपमा वाले या कहानीनुमा सवालों का कक्षा में भी प्रयोग करना शु डिग्री करवाया तो ट्रैक्टन के चुपचाप रहने वाले बच्चे उत्साहपूर्वक कक्षा में भाग लेने लगे। समुदाय की तस्वीरों का इस्तेमाल कर शिक्षक उनसे पूछते - “बताओ जब तुम वहाँ थे तब तुमने क्या किया?” और “वो कैसी चीज़ है?” फिर उन्होंने बच्चों के जवाब रिकॉर्ड किए और स्कूली प्रश्नों को भी टेप में जोड़ा। इन रिकॉर्डिंग को लर्निंग सेंटरों में रखा गया जहाँ बच्चे अपने-आप को सुन पाते और अपने समुदाय की प्रथा के अनुसार उत्तर दे पाते और साथ ही स्कूल के हिसाब से भी उत्तर देते। धीरे-धीरे बच्चों को रिकॉर्डिंग के लिए नए सवाल और जवाब तैयार करना सिखाया गया। इन अनुभवों के ज़रिए जल्दी ही बच्चों को कक्षा के बातचीत के तौर-तरीके समझ में आने लगे। वे यह भी समझने लगे कि स्कूली सवाल-जवाब के तरीके से उनके घरेलू तौर-तरीकों को खतरा नहीं है।
जब शिक्षकों को अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक अनुभवों से उभरी खास बातचीत की रीतियों का ज्ञान होता है, तो वे इन रीतियों को अपनी कक्षा की गतिविधियों में सम्मिलित कर सकते हैं। फिर बच्चों के समुदायों की शिक्षण पद्धति और स्कूली शिक्षा के लिए ज़रूरी शिक्षण पद्धति के बीच असरदार सम्बन्ध तैयार किए जा सकते हैं।
संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास (cognitive development) के ज़्यादातर सिद्धान्तों में सामाजिक और संज्ञानात्मक धाराएँ कम ही जुड़ती हैं। इन्हें एक-दूसरे से जुड़ा हुआ और परस्पर प्रभाव डालने वाला न मानकर यह माना जाता है कि ये एक-दूसरे से अलग काम करती हैं। ज़्यादा-से-ज़्यादा यह माना जाता है कि सामाजिक जगत् संज्ञानात्मक जगत् के लिए एक सन्दर्भ है परन्तु उसका अभिन्न हिस्सा नहीं (Resnik 1991)। प्रारम्भिक बाल्यावस्था विशेषज्ञों की यह मान्यता रही है कि बच्चे जो भी जानते हैं और उनमें जो भी विकास होता है, वह खुद से ही होता है। उसमें सामाजिक तत्वों का कोई हाथ नहीं होता। यह सोच पियाजे द्वारा किए गए काम की देन है। इस सोच के अनुसार जैसे-जैसे बच्चे खुद से भौतिक और सामाजिक जगत् को पहचानते हैं वे इनके बारे में खुद से ही ज्ञान विकसित करते हैं। यह प्रक्रिया सब में अन्तर्निहित होती है। इन्सान में वास्तविकता की समझ एक-जैसी इसलिए होती है क्योंकि इस वास्तविकता को समझने के लिए एक ही जैविक उपकरण है और वह है हमारा दिमाग।
वायगोत्सकी का दृष्टिकोण खास है क्योंकि यह व्यक्ति के दिमाग तक सीमित नहीं है। अपितु देह के बाहर भी फैला हुआ है1 और अन्य दिमागों के साथ जुड़ा हुआ है। वायगोत्सकी के सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धान्त (sociocultural theory) के अनुसार संज्ञान का समाज के साथ एक गहरा सम्बन्ध है। सामाजिक अनुभवों से हमारे सोचने के और दुनिया को समझने के तरीकों पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रभावों से गठित दिमाग में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि एक-दूसरे से बातचीत और मानसिक सम्पर्क का यही मुख्य ज़रिया है। भाषा के द्वारा ही सामाजिक अनुभवों का मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रस्तुतिकरण होता है; यह विचारों को अभिव्यक्त करने का एक ज़रूरी माध्यम है।2 चूँकि वायगोत्सकी के अनुसार भाषा सामाजिक-सांस्कृतिक दुनिया और व्यक्तिगत मानसिक कार्यप्रणाली को जोड़ने वाली सबसे अहम् कड़ी है, इसलिए बच्चों के भाषा सीखने को वे उनके संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानते थे।
सामाजिक योगदान से बनी संज्ञान
वायगोत्सकी के सिद्धान्त की एक मौलिक धारणा यह है कि विशिष्ट रूप से मानवों में पाए जाने वाले उच्च स्तर के मानसिक क्रियाकलाप सामाजिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों से निर्मित होते हैं। इन सामाजिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों के सदस्य इन मानसिक क्रियाकलापों के निर्माण में सहभागी होते हैं क्योंकि ये मानसिक क्रियाकलाप अनुकूलक (adaptive) होते हैं। ये ऐसा ज्ञान और क्षमता देते हैं जो उस विशेष संस्कृति में सफलता के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए समाज-सांस्कृतिक सिद्धान्त मनुष्यों में संज्ञान की क्षमता की विभिन्नता पर बहुत ज़ोर देता है। वायगोत्सकी ने सांस्कृतिक विकास के सामान्य आनुवंशिक नियम (general genetic law of cultural development) में इस विषय पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी व्यक्ति-विशेष के विकास को समझने के लिए उन सामाजिक सम्बन्धों को समझना ज़रूरी है जिनका वो हिस्सा है:
बच्चे के सांस्कृतिक विकास में हरेक क्रिया दो बार या दो स्तरों पर दिखाई देती है। पहले सामाजिक स्तर पर और फिर मनोवैज्ञानिक स्तर पर। पहले वह लोगों के बीच अन्तर-मनोवैज्ञानिक श्रेणी (interpsychological category) के रूप में और फिर बच्चे के अन्दर अन्त:मनोवैज्ञानिक (intrapsychologi-cal) श्रेणी के रूप में दिखाई देती है। यह बात स्वैच्छिक मनोयोग, तार्किक स्मरणशक्ति, अवधारणाओं के गठन, इच्छाशक्ति के विकास, सभी पर लागू होती है। हम इसे किसी कानून की तरह ही मान सकते हैं... इन्सानों में उच्च स्तर के मानसिक क्रियाकलापों और उनके अन्तरसम्बन्धों की आनुवंशिक जड़ में लोगों से लोगों के रिश्ते या सामाजिक सम्बन्ध मौजूद हैं (960ट 1981, 163)।
हालाँकि समाज-सांस्कृतिक दृष्टिकोण सांस्कृतिक विविधता पर ज़ोर देती है, वायगोत्सकी या उनके अनुगामी यह नहीं कहते हैं कि संज्ञान विकास के उन सार्वभौमिक नियमों का अस्तित्व नहीं है जिन्हें हम हर बच्चे में देख पाते हों। बल्कि शोध के भण्डार से भी यह संकेत मिलते हैं कि मानवीय जैविक उपकरण कई सार्वभौमिक संज्ञानात्मक नियमों का स्रोत है। ये संज्ञानात्मक नियम विविध प्रकार के होते हैं, जैसे छोटी आकृतियों को जोड़कर कुछ बनाना, दूसरों की नकल उतारना, चेहरे के हावभाव के मतलब को समझना, यह समझना कि कोई चीज़ अगर छुपी है तो वह गायब नहीं हो गई है, उसका वजूद है और वह फिर नज़र आएगी; और भाषा पर पकड़ हासिल करना।3 समाज-सांस्कृतिक सिद्धान्त यह मानता है कि मानवीय जीववैज्ञानिक क्षमताओं के अलावा कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम हैं जो मनुष्य की सामाजिक प्रकृति और सामाजिक संवाद व आदान-प्रदान के कारण उभरते हैं। उदाहरण के लिए, दुनियाभर में 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे बातचीत में माहिर हो जाते हैं। वे मनुष्यों के संवाद के नियमों का पालन करने लगते हैं, जैसे बातचीत के दौरान एक बोलना बन्द करे तो दूसरे का बोलना (द्यद्वद्धद द्यठ्ठत्त्त्दढ़), आँख मिलाकर बात करना, अपने साथियों द्वारा पूछी गई बातों का ठीक उत्तर देना, बातचीत का प्रसंग जारी रखना।4 ये विकसित संवादात्मक क्षमताएँ शायद देखभाल करने वालों और भाई-बहनों से शैशव अवस्था से बातचीत करने का नतीजा है।
बहरहाल, पिछले कई दशकों से बच्चों के विकास के अध्ययन के क्षेत्र में सार्वभौमिक संज्ञानात्मक पड़ावों की खोज को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके फलस्वरूप संज्ञान के विकास में सामाजिक तथ्यों की भूमिका पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है (Wertsch 1991a)। आजकल विकासात्मक मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद् यह मानने लगे हैं कि सामाजिक और संज्ञानात्मक एक-दूसरे के आवश्यक पहलू हैं। बढ़ते हुए प्रमाण ये दिखाते हैं कि सार्वभौमिक माने जाने वाले संज्ञानात्मक गुणों में सामाजिक प्रभाव हमेशा गुँथे रहते हैं और बच्चों के चिन्तन को बदलने में सामाजिक जुड़ाव (social engagement) का बड़ा हाथ है। इन प्रमाणों के कारण बाल विकास विशेषज्ञ यह मानने लगे हैं कि संज्ञान सामाजिक स्थितियों में बसी है।
सामाजिक सन्दर्भों में बसे संज्ञानात्मक कौशल: सामाजिक अन्तरक्रिया
संरक्षण सिद्धान्त पर अध्ययनों की आजकल भरमार है। संख्या, आयतन मात्रा आदि का संरक्षण पियाजे द्वारा स्थापित किया गया वह पड़ाव है जहाँ बालसुलभ तर्कहीन सोच परिपक्व तार्किक सोच में बदलती है। इनमें से कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि संरक्षण वाले कामों के लिए वयस्कों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बच्चे सामाजिक चश्मों (social lenses) से देखते हैं, जिससे उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है (Resnick 1991,5)।
हमने पहले ही देखा है कि पारस्परिक बातचीत से बच्चे रोज़मर्रा की बातचीत के कई तौर-तरीके सीख जाते हैं। वे ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं कि बातचीत के दौरान साथी उनसे जो कह रहे हैं वह प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होगा। संरक्षण विषयक सवाल-जवाब में इन तौर तरीकों से हटकर बातचीत करने की ज़रूरत को वे समझ नहीं पाते। संरक्षण के बारे में बच्चों से सवाल-जवाब करते वक्त ऐेसे विषयों पर बातचीत की जाती है जिनमें रोज़मर्रा की ज़िन्दगी की बातचीत के दौरान खास रुचि नहीं ली जाती। एक ही सवाल बार-बार दोहराया जाता है, यह समझने के लिए कि बच्चे जो उत्तर दे रहे हैं वे उसके बारे में निश्चित हैं या नहीं, उनके जवाब उनकी सोच को ठीक-ठीक व्यक्त करते हैं कि नहीं। इससे बच्चे सवालों को गलत समझ सकते हैं -- इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें उत्तर नहीं मालूम बल्कि इसलिए क्योंकि उनके और बड़ों के बीच बातचीत के नियमों का तालमेल नहीं बन पाया है।
एक ही प्रश्न को बार-बार दोहराना संरक्षण की जाँच के लिए किए गए सवाल-जवाब का एक खास पहलू है। उदाहरण के लिए तरल पदार्थों के संरक्षण की समस्या को लीजिए जिसमें दो अलग आकार के पात्र लिए जाते हैं और एक पात्र से पानी दूसरे में डाला जाता है। फिर बच्चे से पूछा जाता है कि क्या पानी की मात्रा में कोई बदलाव है। जब किसी बच्चे को यह सवाल एक से ज़्यादा बार पूछा जाता है तो उसे लगता है कि शायद पहला जवाब सही नहीं था, इसलिए उससे फिर पूछा जा रहा है। सोचिए, जब आपके सहकर्मी आपसे पूछते हैं, “आप कैसे हैं” या “आपकी छुट्टी कैसी गुज़री?”, और वे बार-बार आपसे यही पूछते जाएँ तो आपको भी लगेगा कि वो आपसे कुछ और सुनना चाहते हैं और आप बदल-बदलकर जवाब देंगे। सीगल, वॉटर्स और डिनविडी द्वारा किए गए शोधों से हमें यह पता लगा है कि बच्चे कुछ इसी तरह की सामाजिक-दृष्टि संरक्षण सम्बन्धी वार्तालाप की स्थितियों में लाते हैं।5
एक शुरुआती प्रयोग में 4 से 6 साल के 180 बच्चों को दो दलों में बाँटा गया। उनसे संख्या संरक्षण के सवाल पूछे गए। इसमें बच्चों से जानने की कोशिश की जाती है कि क्या वे यह समझ पाते हैं कि दो अलग लम्बाई की पंक्तियों में समान संख्या के बटन रखे गए हैं। एक दल के बच्चों से बटनों को इधर-उधर करने से पहले और बाद में यह प्रश्न किया गया, और दूसरे दल से यह प्रश्न सिर्फ एक बार किया गया -- बटन इधर-उधर करने के बाद। एक प्रश्न वाले दल में से 78% बच्चों ने सही जवाब दिया (यानी उनके जवाब संख्या संरक्षण के नियमानुसार थे), जबकि दो प्रश्न वाले दल में से केवल 28% बच्चे ही ठीक जवाब दे पाए।
एक और शोध में कुछ बच्चों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कठपुतलियों से संख्या संरक्षण के सवाल पूछे जा रहे थे - कुछ कठपुतलियों से एक बार और कुछ से दो बार। फिर बच्चों से यह पूछा गया कि कठपुतलियाँ जो जवाब दे रही थीं क्या वो बड़ों को ‘खुश करने के लिए’ थे या वे ‘वही बता रही थीं जो उन्हें सही लगता था’। 69% बच्चों को लगा कि दो सवाल वाली स्थिति में जो कठपुतलियाँ संरक्षण के विपरीत उत्तर दे रही थीं, वे बड़ों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही थीं। इसके विपरीत सिर्फ 44% बच्चों को लगा कि एक सवाल वाले समूह में जो कठपुतलियाँ संरक्षण के विपरीत उत्तर दे रही थीं, वे बड़ों को खुश करने के लिए दे रही थीं। यह दिखाने के लिए कि 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे रोज़मर्रा की बातचीत के कायदे संरक्षण सम्बन्धी बातचीत में भी लागू करते हैं, एक और अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में पहले एक वयस्क ने बच्चों से प्रश्न किया, फिर चीज़ों को इधर-उधर करने के बाद एक दूसरे वयस्क ने बच्चों से प्रश्न किया। इस स्थिति में ज़्यादा बच्चों ने संरक्षण के सिद्धान्त के अनुरूप उत्तर दिए।
सार यह है कि बच्चे साक्षात्कार यानी सवाल-जवाब की स्थिति में उनके सामाजिक अनुभवों से विकसित धारणाएँ और विचार लेकर आते हैं। बड़ों द्वारा उनको दिए गए संज्ञानात्मक कार्य को समझने के अलावा वे इस कार्य को घेरे हुए सामाजिक सम्बन्धों को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब बड़े यह समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे उनके प्रश्न करने के तरीके से भ्रम में पड़ सकते हैं, तो इसकी सम्भावना बढ़ जाती है कि वे बच्चों के ज्ञान और योग्यता का अनुमान ठीक से न लगा पाएँ।
कभी-कभी बड़ों के सवाल करने के तरीके सामाजिक मेलजोल के तरीकों के बारे में व्याप्त गहरी अपेक्षाओं के बिलकुल उलट होते हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों में बड़ों का बच्चों से सीखने-सिखाने वाले सवाल (instructional questions) पूछना आम है। जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि ‘यह गाड़ी कौन-से रंग की है’ या ‘तुम्हारे ढेर में क्या उतने ही पैसे हैं जितने मेरे ढेर में?’ पर इस तरह के प्रश्न करने का प्रचलन अन्य समुदायों में नहीं है। वहाँ वार्तालाप के और ही तौर-तरीके होते हैं।
यह उदाहरण समाज-सांस्कृतिक सिद्धान्त के एक और आधार को सामने लाता है -- हमारे सोचने के तरीके हमारे सामाजिक सन्दर्भ में बसे हुए हैं, सिर्फ दो लोगों के बीच (द्विक/dyad) या छोटे समूहों के स्तर पर ही नहीं बल्कि उन वृहत् संस्थानिक और सांस्कृतिक स्तरों पर भी जिनमें आमने-सामने की जाने वाली बातचीत बसी हुई हैं।7 मध्यमवर्गीय माता-पिताओं के ‘सिखाने वाले सवाल’ स्कूली सवाल-जवाब के तरीकों से मेल खाते हैं। इससे इन परिवारों के बच्चे कक्षाओं में और परीक्षा की स्थितियों में अच्छी तरह से बातचीत कर पाते हैं। कई शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि पश्चिम के देशों में गैर-मध्यमवर्गीय बच्चों को कक्षा में बातचीत करने में जो दिक्कतें आती हैं वे उनके घरों में हो रही बातचीत के तरीकों और स्कूलों में बातचीत के तरीकों के बेमेलपन के कारण होता है।8 नतीजतन शिक्षकों को कक्षा में कुछ ऐसे बदलाव लाने पड़ेंगे जिससे अलग-अलग संस्कृतियों से (खासकर अल्पसंख्यक या हाशिए पर धकेले गए समुदायों या संस्कृतियों से) आने वाले बच्चे भी कक्षा की गतिविधियों में शामिल हो सकें और शिक्षक इन बच्चों के सामाजिक इतिहास का कक्षा में समुचित उपयोग कर सकें।
संज्ञानात्मक कौशलों की सामाजिक गुँथन: कार्य और उसकी परिस्थितियाँ
वृहत सामाजिक सन्दर्भ का संज्ञान पर प्रभाव तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम कार्य की प्रकृति को बच्चों के सामाजिक अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए हम फिर संरक्षण के सवालों पर लौटते हैं। इस बात के बहुत प्रमाण मिले हैं कि पाश्चात्य सभ्यता से इतर आदिवासी और ग्रामीण समाज के बच्चों में संरक्षण की क्षमता अक्सर बहुत देर से आती है। उदाहरण के तौर पर नाइजेरिया के हौसा लोगों को लें जो छोटी कृषि बस्तियों में रहते हैं, अपने बच्चों को कम ही स्कूल भेजते हैं। इन बच्चों को सबसे सरल संरक्षण कार्य (यानी अंक, लम्बाई और द्रव्य का संरक्षण) 11 साल या उसके भी बाद समझ आते हैं (Fahrmeier1978)। यह इसके बावजूद कि हौसा बच्चों के रोज़मर्रा के परिवेश काफी उत्तेजक/उत्प्रेरक हैं जो पियाजे के अनुसार ठोस क्रियात्मक चरण (concrete operational stage) पर जाने का अनुभवजन्य मानदण्ड है।
अलग-अलग संस्कृतियों में संरक्षण की स्थिति तक पहुँचने में इस बड़ी असमानता को कैसे समझा जाए? लाइट और पैरेट-क्लेरमोंट (Light and Perret-Clermont 1980) के अनुसार संरक्षण व ऐसी ही अन्य अवधारणाओं में दक्षता पाने के लिए बच्चों को रोज़ ऐसे कार्यों में भाग लेना चाहिए जो इस तरह की सोच को बढ़ावा दे सकें। जैसे, पाश्चात्य देशों के बच्चों के लिए निष्पक्षता का अभिप्राय संसाधन का समान वितरण बन गया है। उन्हें अपनी चीज़ों को बाँटने के कई मौके मिलते हैं, जैसे क्रेयॉन या त्यौहार पर मिली हुई मिठाइयाँ और तोहफे। इसके कारण वे एक ही मात्रा की चीज़ों को अलग-अलग तरीकों से बँटते देखते हैं और संरक्षण के सिद्धान्त को जल्दी पकड़ लेते हैं। पर ऐसी संस्कृतियों में जहाँ इस तरह के अनुभवों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ कम ही होती हैं, वहाँ पाश्चात्य सभ्यताओं में संरक्षण हासिल करने वाली उम्र में ही बच्चों में संरक्षण की स्थिति के आने की सम्भावना कम है।
संज्ञानात्मक कार्य से जुड़े ऐसे और भी निष्कर्ष हैं जिनके बारे में यह सोचा जाता था कि उन पर विशिष्ट अनुभव और प्रथा का कम ही असर पड़ता है। वेशलर द्वारा निर्मित बच्चों की बुद्धिमत्ता मापन के संवर्धित पैमाने9 की ब्लॉक डिज़ाइन उप-परीक्षा एक ऐसा उदाहरण है। इसे सांस्कृतिक तौर पर निष्पक्ष माना जाता है और स्थानिक समझ (spatial reasoning) को परखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक शोध में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को ब्लॉक डिज़ाइन के काम दिए गए। इस कार्य में बच्चों के प्रदर्शन को इस बात से जोड़ा गया कि उन्होंने बाज़ार में मिलने वाले इस तरह के महँगे खिलौनों से कितनी बार खेला था। उनको दिए गए कार्य और ऐसे गेम -- दोनों में ही छोटे घनों (क्यूब) को जोड़कर एक आकृति की जल्द-से-जल्द नकल बनानी थी (Dirks 1982)। निम्नवर्गीय, अल्पसंख्यक बच्चे जो वस्तु-केन्द्रित नहीं, बल्की मानव-केन्द्रित घरों में पलते हैं, उनमें ऐसे खेलों और चीज़ों से खेलने से मिलने वाले अनुभवों और कौशलों की कमी होने की सम्भावना है (ओकागाकी व स्टाइनबर्ग, 1993)।
वायगोत्सकी और उनके सहकर्मी संज्ञानात्मक विकास में स्कूली शिक्षण और उससे जुड़े क्रियाकलापों के असर के बारे में अच्छी तरह वाकिफ थे (Luria 1976)। वायगोत्सकी के अनुसार शैक्षिक कार्यों में दक्षता हासिल करने से बच्चों की स्मृतिशक्ति, अवधारणाओं का बनना, तर्कबुद्धि और समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होती है -- जैसा कि नए शोध भी साबित कर चुके हैं (Ceci 1990, 1991)। कक्षाओं में जिस तरह के ज्ञानार्जन की अपेक्षा की जाती है, उसके साथ इस तरह के विकासात्मक परिवर्तनों का जुड़ाव ज़ाहिर है। पर स्कूल से बाहर किए जाने वाले प्रायोगिक कार्यों में ये बातें लागू नहीं होतीं।
उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 9 साल की उम्र के अमरीकी बच्चों से खेल के मैदान में रखी 40 चीज़ों की जगहों को याद रखने को कहा। ये बच्चे इन चीज़ों के नामों को बार-बार दोहराकर याद रखने की कोशिश करने लगे। असंगत चीज़ों को याद रखने के लिए इस्तेमाल की गई यह स्कूली पद्धति यहाँ असफल रही। इसके विपरीत ग्वातेमाला के माया बच्चे इसी कार्य को बेहतर कर पाए। पर जब माया बच्चों को असंगत चीज़ों की सूची को याद रखने का कार्य दिया गया तो वे उतनी अच्छी तरह से यह कार्य नहीं कर पाए (रॉगॉफ एवं वैडेल)।
ये सारे निष्कर्ष हमें बताते हैं कि सभी संस्कृतियों के बच्चों को सामान्यत: एक ही तरह के कार्यों से नहीं जूझना पड़ता। संस्कृतियाँ और उनमें बसे सामाजिकता के कायदे-कानून बच्चों को सिखाने के अलग-अलग कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। इसके कारण बच्चों का संज्ञान, जो सन्दर्भ-आधारित (contextualised) होता है, विभिन्न कार्यों और सामाजिक अनुभवों से उत्पन्न होता है।
सार यह है कि समाज-सांस्कृतिक सिद्धान्त के अनुसार सोच-विचार की जिन क्षमताओं को शुरुआती और मध्य बाल्यावस्था में विकसित होने वाला माना जाता है, वे खास सन्दर्भों और सांस्कृतिक स्थितियों की उपज हैं। जितना पहले माना जाता था, उससे कहीं ज़्यादा।
जब हीथ ने शिक्षकों से इस तरह के उपमा वाले या कहानीनुमा सवालों का कक्षा में भी प्रयोग करना शु डिग्री करवाया तो ट्रैक्टन के चुपचाप रहने वाले बच्चे उत्साहपूर्वक कक्षा में भाग लेने लगे। समुदाय की तस्वीरों का इस्तेमाल कर शिक्षक उनसे पूछते - “बताओ जब तुम वहाँ थे तब तुमने क्या किया?” और “वो कैसी चीज़ है?” फिर उन्होंने बच्चों के जवाब रिकॉर्ड किए और स्कूली प्रश्नों को भी टेप में जोड़ा। इन रिकॉर्डिंग को लर्निंग सेंटरों में रखा गया जहाँ बच्चे अपने-आप को सुन पाते और अपने समुदाय की प्रथा के अनुसार उत्तर दे पाते और साथ ही स्कूल के हिसाब से भी उत्तर देते। धीरे-धीरे बच्चों को रिकॉर्डिंग के लिए नए सवाल और जवाब तैयार करना सिखाया गया। इन अनुभवों के ज़रिए जल्दी ही बच्चों को कक्षा के बातचीत के तौर-तरीके समझ में आने लगे। वे यह भी समझने लगे कि स्कूली सवाल-जवाब के तरीके से उनके घरेलू तौर-तरीकों को खतरा नहीं है।
जब शिक्षकों को अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक अनुभवों से उभरी खास बातचीत की रीतियों का ज्ञान होता है, तो वे इन रीतियों को अपनी कक्षा की गतिविधियों में सम्मिलित कर सकते हैं। फिर बच्चों के समुदायों की शिक्षण पद्धति और स्कूली शिक्षा के लिए ज़रूरी शिक्षण पद्धति के बीच असरदार सम्बन्ध तैयार किए जा सकते हैं।
संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास (cognitive development) के ज़्यादातर सिद्धान्तों में सामाजिक और संज्ञानात्मक धाराएँ कम ही जुड़ती हैं। इन्हें एक-दूसरे से जुड़ा हुआ और परस्पर प्रभाव डालने वाला न मानकर यह माना जाता है कि ये एक-दूसरे से अलग काम करती हैं। ज़्यादा-से-ज़्यादा यह माना जाता है कि सामाजिक जगत् संज्ञानात्मक जगत् के लिए एक सन्दर्भ है परन्तु उसका अभिन्न हिस्सा नहीं (Resnik 1991)। प्रारम्भिक बाल्यावस्था विशेषज्ञों की यह मान्यता रही है कि बच्चे जो भी जानते हैं और उनमें जो भी विकास होता है, वह खुद से ही होता है। उसमें सामाजिक तत्वों का कोई हाथ नहीं होता। यह सोच पियाजे द्वारा किए गए काम की देन है। इस सोच के अनुसार जैसे-जैसे बच्चे खुद से भौतिक और सामाजिक जगत् को पहचानते हैं वे इनके बारे में खुद से ही ज्ञान विकसित करते हैं। यह प्रक्रिया सब में अन्तर्निहित होती है। इन्सान में वास्तविकता की समझ एक-जैसी इसलिए होती है क्योंकि इस वास्तविकता को समझने के लिए एक ही जैविक उपकरण है और वह है हमारा दिमाग।
वायगोत्सकी का दृष्टिकोण खास है क्योंकि यह व्यक्ति के दिमाग तक सीमित नहीं है। अपितु देह के बाहर भी फैला हुआ है1 और अन्य दिमागों के साथ जुड़ा हुआ है। वायगोत्सकी के सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धान्त (sociocultural theory) के अनुसार संज्ञान का समाज के साथ एक गहरा सम्बन्ध है। सामाजिक अनुभवों से हमारे सोचने के और दुनिया को समझने के तरीकों पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रभावों से गठित दिमाग में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि एक-दूसरे से बातचीत और मानसिक सम्पर्क का यही मुख्य ज़रिया है। भाषा के द्वारा ही सामाजिक अनुभवों का मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रस्तुतिकरण होता है; यह विचारों को अभिव्यक्त करने का एक ज़रूरी माध्यम है।2 चूँकि वायगोत्सकी के अनुसार भाषा सामाजिक-सांस्कृतिक दुनिया और व्यक्तिगत मानसिक कार्यप्रणाली को जोड़ने वाली सबसे अहम् कड़ी है, इसलिए बच्चों के भाषा सीखने को वे उनके संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानते थे।
सामाजिक योगदान से बनी संज्ञान
वायगोत्सकी के सिद्धान्त की एक मौलिक धारणा यह है कि विशिष्ट रूप से मानवों में पाए जाने वाले उच्च स्तर के मानसिक क्रियाकलाप सामाजिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों से निर्मित होते हैं। इन सामाजिक और सांस्कृतिक सन्दर्भों के सदस्य इन मानसिक क्रियाकलापों के निर्माण में सहभागी होते हैं क्योंकि ये मानसिक क्रियाकलाप अनुकूलक (adaptive) होते हैं। ये ऐसा ज्ञान और क्षमता देते हैं जो उस विशेष संस्कृति में सफलता के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए समाज-सांस्कृतिक सिद्धान्त मनुष्यों में संज्ञान की क्षमता की विभिन्नता पर बहुत ज़ोर देता है। वायगोत्सकी ने सांस्कृतिक विकास के सामान्य आनुवंशिक नियम (general genetic law of cultural development) में इस विषय पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी व्यक्ति-विशेष के विकास को समझने के लिए उन सामाजिक सम्बन्धों को समझना ज़रूरी है जिनका वो हिस्सा है:
बच्चे के सांस्कृतिक विकास में हरेक क्रिया दो बार या दो स्तरों पर दिखाई देती है। पहले सामाजिक स्तर पर और फिर मनोवैज्ञानिक स्तर पर। पहले वह लोगों के बीच अन्तर-मनोवैज्ञानिक श्रेणी (interpsychological category) के रूप में और फिर बच्चे के अन्दर अन्त:मनोवैज्ञानिक (intrapsychologi-cal) श्रेणी के रूप में दिखाई देती है। यह बात स्वैच्छिक मनोयोग, तार्किक स्मरणशक्ति, अवधारणाओं के गठन, इच्छाशक्ति के विकास, सभी पर लागू होती है। हम इसे किसी कानून की तरह ही मान सकते हैं... इन्सानों में उच्च स्तर के मानसिक क्रियाकलापों और उनके अन्तरसम्बन्धों की आनुवंशिक जड़ में लोगों से लोगों के रिश्ते या सामाजिक सम्बन्ध मौजूद हैं (960ट 1981, 163)।
हालाँकि समाज-सांस्कृतिक दृष्टिकोण सांस्कृतिक विविधता पर ज़ोर देती है, वायगोत्सकी या उनके अनुगामी यह नहीं कहते हैं कि संज्ञान विकास के उन सार्वभौमिक नियमों का अस्तित्व नहीं है जिन्हें हम हर बच्चे में देख पाते हों। बल्कि शोध के भण्डार से भी यह संकेत मिलते हैं कि मानवीय जैविक उपकरण कई सार्वभौमिक संज्ञानात्मक नियमों का स्रोत है। ये संज्ञानात्मक नियम विविध प्रकार के होते हैं, जैसे छोटी आकृतियों को जोड़कर कुछ बनाना, दूसरों की नकल उतारना, चेहरे के हावभाव के मतलब को समझना, यह समझना कि कोई चीज़ अगर छुपी है तो वह गायब नहीं हो गई है, उसका वजूद है और वह फिर नज़र आएगी; और भाषा पर पकड़ हासिल करना।3 समाज-सांस्कृतिक सिद्धान्त यह मानता है कि मानवीय जीववैज्ञानिक क्षमताओं के अलावा कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम हैं जो मनुष्य की सामाजिक प्रकृति और सामाजिक संवाद व आदान-प्रदान के कारण उभरते हैं। उदाहरण के लिए, दुनियाभर में 2 से 3 साल की उम्र के बच्चे बातचीत में माहिर हो जाते हैं। वे मनुष्यों के संवाद के नियमों का पालन करने लगते हैं, जैसे बातचीत के दौरान एक बोलना बन्द करे तो दूसरे का बोलना (द्यद्वद्धद द्यठ्ठत्त्त्दढ़), आँख मिलाकर बात करना, अपने साथियों द्वारा पूछी गई बातों का ठीक उत्तर देना, बातचीत का प्रसंग जारी रखना।4 ये विकसित संवादात्मक क्षमताएँ शायद देखभाल करने वालों और भाई-बहनों से शैशव अवस्था से बातचीत करने का नतीजा है।
बहरहाल, पिछले कई दशकों से बच्चों के विकास के अध्ययन के क्षेत्र में सार्वभौमिक संज्ञानात्मक पड़ावों की खोज को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके फलस्वरूप संज्ञान के विकास में सामाजिक तथ्यों की भूमिका पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है (Wertsch 1991a)। आजकल विकासात्मक मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद् यह मानने लगे हैं कि सामाजिक और संज्ञानात्मक एक-दूसरे के आवश्यक पहलू हैं। बढ़ते हुए प्रमाण ये दिखाते हैं कि सार्वभौमिक माने जाने वाले संज्ञानात्मक गुणों में सामाजिक प्रभाव हमेशा गुँथे रहते हैं और बच्चों के चिन्तन को बदलने में सामाजिक जुड़ाव (social engagement) का बड़ा हाथ है। इन प्रमाणों के कारण बाल विकास विशेषज्ञ यह मानने लगे हैं कि संज्ञान सामाजिक स्थितियों में बसी है।
सामाजिक सन्दर्भों में बसे संज्ञानात्मक कौशल: सामाजिक अन्तरक्रिया
संरक्षण सिद्धान्त पर अध्ययनों की आजकल भरमार है। संख्या, आयतन मात्रा आदि का संरक्षण पियाजे द्वारा स्थापित किया गया वह पड़ाव है जहाँ बालसुलभ तर्कहीन सोच परिपक्व तार्किक सोच में बदलती है। इनमें से कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि संरक्षण वाले कामों के लिए वयस्कों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बच्चे सामाजिक चश्मों (social lenses) से देखते हैं, जिससे उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ता है (Resnick 1991,5)।
हमने पहले ही देखा है कि पारस्परिक बातचीत से बच्चे रोज़मर्रा की बातचीत के कई तौर-तरीके सीख जाते हैं। वे ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं कि बातचीत के दौरान साथी उनसे जो कह रहे हैं वह प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होगा। संरक्षण विषयक सवाल-जवाब में इन तौर तरीकों से हटकर बातचीत करने की ज़रूरत को वे समझ नहीं पाते। संरक्षण के बारे में बच्चों से सवाल-जवाब करते वक्त ऐेसे विषयों पर बातचीत की जाती है जिनमें रोज़मर्रा की ज़िन्दगी की बातचीत के दौरान खास रुचि नहीं ली जाती। एक ही सवाल बार-बार दोहराया जाता है, यह समझने के लिए कि बच्चे जो उत्तर दे रहे हैं वे उसके बारे में निश्चित हैं या नहीं, उनके जवाब उनकी सोच को ठीक-ठीक व्यक्त करते हैं कि नहीं। इससे बच्चे सवालों को गलत समझ सकते हैं -- इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें उत्तर नहीं मालूम बल्कि इसलिए क्योंकि उनके और बड़ों के बीच बातचीत के नियमों का तालमेल नहीं बन पाया है।
एक ही प्रश्न को बार-बार दोहराना संरक्षण की जाँच के लिए किए गए सवाल-जवाब का एक खास पहलू है। उदाहरण के लिए तरल पदार्थों के संरक्षण की समस्या को लीजिए जिसमें दो अलग आकार के पात्र लिए जाते हैं और एक पात्र से पानी दूसरे में डाला जाता है। फिर बच्चे से पूछा जाता है कि क्या पानी की मात्रा में कोई बदलाव है। जब किसी बच्चे को यह सवाल एक से ज़्यादा बार पूछा जाता है तो उसे लगता है कि शायद पहला जवाब सही नहीं था, इसलिए उससे फिर पूछा जा रहा है। सोचिए, जब आपके सहकर्मी आपसे पूछते हैं, “आप कैसे हैं” या “आपकी छुट्टी कैसी गुज़री?”, और वे बार-बार आपसे यही पूछते जाएँ तो आपको भी लगेगा कि वो आपसे कुछ और सुनना चाहते हैं और आप बदल-बदलकर जवाब देंगे। सीगल, वॉटर्स और डिनविडी द्वारा किए गए शोधों से हमें यह पता लगा है कि बच्चे कुछ इसी तरह की सामाजिक-दृष्टि संरक्षण सम्बन्धी वार्तालाप की स्थितियों में लाते हैं।5
एक शुरुआती प्रयोग में 4 से 6 साल के 180 बच्चों को दो दलों में बाँटा गया। उनसे संख्या संरक्षण के सवाल पूछे गए। इसमें बच्चों से जानने की कोशिश की जाती है कि क्या वे यह समझ पाते हैं कि दो अलग लम्बाई की पंक्तियों में समान संख्या के बटन रखे गए हैं। एक दल के बच्चों से बटनों को इधर-उधर करने से पहले और बाद में यह प्रश्न किया गया, और दूसरे दल से यह प्रश्न सिर्फ एक बार किया गया -- बटन इधर-उधर करने के बाद। एक प्रश्न वाले दल में से 78% बच्चों ने सही जवाब दिया (यानी उनके जवाब संख्या संरक्षण के नियमानुसार थे), जबकि दो प्रश्न वाले दल में से केवल 28% बच्चे ही ठीक जवाब दे पाए।
एक और शोध में कुछ बच्चों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कठपुतलियों से संख्या संरक्षण के सवाल पूछे जा रहे थे - कुछ कठपुतलियों से एक बार और कुछ से दो बार। फिर बच्चों से यह पूछा गया कि कठपुतलियाँ जो जवाब दे रही थीं क्या वो बड़ों को ‘खुश करने के लिए’ थे या वे ‘वही बता रही थीं जो उन्हें सही लगता था’। 69% बच्चों को लगा कि दो सवाल वाली स्थिति में जो कठपुतलियाँ संरक्षण के विपरीत उत्तर दे रही थीं, वे बड़ों को खुश करने के लिए ऐसा कर रही थीं। इसके विपरीत सिर्फ 44% बच्चों को लगा कि एक सवाल वाले समूह में जो कठपुतलियाँ संरक्षण के विपरीत उत्तर दे रही थीं, वे बड़ों को खुश करने के लिए दे रही थीं। यह दिखाने के लिए कि 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे रोज़मर्रा की बातचीत के कायदे संरक्षण सम्बन्धी बातचीत में भी लागू करते हैं, एक और अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में पहले एक वयस्क ने बच्चों से प्रश्न किया, फिर चीज़ों को इधर-उधर करने के बाद एक दूसरे वयस्क ने बच्चों से प्रश्न किया। इस स्थिति में ज़्यादा बच्चों ने संरक्षण के सिद्धान्त के अनुरूप उत्तर दिए।
सार यह है कि बच्चे साक्षात्कार यानी सवाल-जवाब की स्थिति में उनके सामाजिक अनुभवों से विकसित धारणाएँ और विचार लेकर आते हैं। बड़ों द्वारा उनको दिए गए संज्ञानात्मक कार्य को समझने के अलावा वे इस कार्य को घेरे हुए सामाजिक सम्बन्धों को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब बड़े यह समझ नहीं पाते हैं कि बच्चे उनके प्रश्न करने के तरीके से भ्रम में पड़ सकते हैं, तो इसकी सम्भावना बढ़ जाती है कि वे बच्चों के ज्ञान और योग्यता का अनुमान ठीक से न लगा पाएँ।
कभी-कभी बड़ों के सवाल करने के तरीके सामाजिक मेलजोल के तरीकों के बारे में व्याप्त गहरी अपेक्षाओं के बिलकुल उलट होते हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों में बड़ों का बच्चों से सीखने-सिखाने वाले सवाल (instructional questions) पूछना आम है। जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि ‘यह गाड़ी कौन-से रंग की है’ या ‘तुम्हारे ढेर में क्या उतने ही पैसे हैं जितने मेरे ढेर में?’ पर इस तरह के प्रश्न करने का प्रचलन अन्य समुदायों में नहीं है। वहाँ वार्तालाप के और ही तौर-तरीके होते हैं।
यह उदाहरण समाज-सांस्कृतिक सिद्धान्त के एक और आधार को सामने लाता है -- हमारे सोचने के तरीके हमारे सामाजिक सन्दर्भ में बसे हुए हैं, सिर्फ दो लोगों के बीच (द्विक/dyad) या छोटे समूहों के स्तर पर ही नहीं बल्कि उन वृहत् संस्थानिक और सांस्कृतिक स्तरों पर भी जिनमें आमने-सामने की जाने वाली बातचीत बसी हुई हैं।7 मध्यमवर्गीय माता-पिताओं के ‘सिखाने वाले सवाल’ स्कूली सवाल-जवाब के तरीकों से मेल खाते हैं। इससे इन परिवारों के बच्चे कक्षाओं में और परीक्षा की स्थितियों में अच्छी तरह से बातचीत कर पाते हैं। कई शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि पश्चिम के देशों में गैर-मध्यमवर्गीय बच्चों को कक्षा में बातचीत करने में जो दिक्कतें आती हैं वे उनके घरों में हो रही बातचीत के तरीकों और स्कूलों में बातचीत के तरीकों के बेमेलपन के कारण होता है।8 नतीजतन शिक्षकों को कक्षा में कुछ ऐसे बदलाव लाने पड़ेंगे जिससे अलग-अलग संस्कृतियों से (खासकर अल्पसंख्यक या हाशिए पर धकेले गए समुदायों या संस्कृतियों से) आने वाले बच्चे भी कक्षा की गतिविधियों में शामिल हो सकें और शिक्षक इन बच्चों के सामाजिक इतिहास का कक्षा में समुचित उपयोग कर सकें।
संज्ञानात्मक कौशलों की सामाजिक गुँथन: कार्य और उसकी परिस्थितियाँ
वृहत सामाजिक सन्दर्भ का संज्ञान पर प्रभाव तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम कार्य की प्रकृति को बच्चों के सामाजिक अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए हम फिर संरक्षण के सवालों पर लौटते हैं। इस बात के बहुत प्रमाण मिले हैं कि पाश्चात्य सभ्यता से इतर आदिवासी और ग्रामीण समाज के बच्चों में संरक्षण की क्षमता अक्सर बहुत देर से आती है। उदाहरण के तौर पर नाइजेरिया के हौसा लोगों को लें जो छोटी कृषि बस्तियों में रहते हैं, अपने बच्चों को कम ही स्कूल भेजते हैं। इन बच्चों को सबसे सरल संरक्षण कार्य (यानी अंक, लम्बाई और द्रव्य का संरक्षण) 11 साल या उसके भी बाद समझ आते हैं (Fahrmeier1978)। यह इसके बावजूद कि हौसा बच्चों के रोज़मर्रा के परिवेश काफी उत्तेजक/उत्प्रेरक हैं जो पियाजे के अनुसार ठोस क्रियात्मक चरण (concrete operational stage) पर जाने का अनुभवजन्य मानदण्ड है।
अलग-अलग संस्कृतियों में संरक्षण की स्थिति तक पहुँचने में इस बड़ी असमानता को कैसे समझा जाए? लाइट और पैरेट-क्लेरमोंट (Light and Perret-Clermont 1980) के अनुसार संरक्षण व ऐसी ही अन्य अवधारणाओं में दक्षता पाने के लिए बच्चों को रोज़ ऐसे कार्यों में भाग लेना चाहिए जो इस तरह की सोच को बढ़ावा दे सकें। जैसे, पाश्चात्य देशों के बच्चों के लिए निष्पक्षता का अभिप्राय संसाधन का समान वितरण बन गया है। उन्हें अपनी चीज़ों को बाँटने के कई मौके मिलते हैं, जैसे क्रेयॉन या त्यौहार पर मिली हुई मिठाइयाँ और तोहफे। इसके कारण वे एक ही मात्रा की चीज़ों को अलग-अलग तरीकों से बँटते देखते हैं और संरक्षण के सिद्धान्त को जल्दी पकड़ लेते हैं। पर ऐसी संस्कृतियों में जहाँ इस तरह के अनुभवों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ कम ही होती हैं, वहाँ पाश्चात्य सभ्यताओं में संरक्षण हासिल करने वाली उम्र में ही बच्चों में संरक्षण की स्थिति के आने की सम्भावना कम है।
संज्ञानात्मक कार्य से जुड़े ऐसे और भी निष्कर्ष हैं जिनके बारे में यह सोचा जाता था कि उन पर विशिष्ट अनुभव और प्रथा का कम ही असर पड़ता है। वेशलर द्वारा निर्मित बच्चों की बुद्धिमत्ता मापन के संवर्धित पैमाने9 की ब्लॉक डिज़ाइन उप-परीक्षा एक ऐसा उदाहरण है। इसे सांस्कृतिक तौर पर निष्पक्ष माना जाता है और स्थानिक समझ (spatial reasoning) को परखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक शोध में प्राथमिक स्कूल के बच्चों को ब्लॉक डिज़ाइन के काम दिए गए। इस कार्य में बच्चों के प्रदर्शन को इस बात से जोड़ा गया कि उन्होंने बाज़ार में मिलने वाले इस तरह के महँगे खिलौनों से कितनी बार खेला था। उनको दिए गए कार्य और ऐसे गेम -- दोनों में ही छोटे घनों (क्यूब) को जोड़कर एक आकृति की जल्द-से-जल्द नकल बनानी थी (Dirks 1982)। निम्नवर्गीय, अल्पसंख्यक बच्चे जो वस्तु-केन्द्रित नहीं, बल्की मानव-केन्द्रित घरों में पलते हैं, उनमें ऐसे खेलों और चीज़ों से खेलने से मिलने वाले अनुभवों और कौशलों की कमी होने की सम्भावना है (ओकागाकी व स्टाइनबर्ग, 1993)।
वायगोत्सकी और उनके सहकर्मी संज्ञानात्मक विकास में स्कूली शिक्षण और उससे जुड़े क्रियाकलापों के असर के बारे में अच्छी तरह वाकिफ थे (Luria 1976)। वायगोत्सकी के अनुसार शैक्षिक कार्यों में दक्षता हासिल करने से बच्चों की स्मृतिशक्ति, अवधारणाओं का बनना, तर्कबुद्धि और समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होती है -- जैसा कि नए शोध भी साबित कर चुके हैं (Ceci 1990, 1991)। कक्षाओं में जिस तरह के ज्ञानार्जन की अपेक्षा की जाती है, उसके साथ इस तरह के विकासात्मक परिवर्तनों का जुड़ाव ज़ाहिर है। पर स्कूल से बाहर किए जाने वाले प्रायोगिक कार्यों में ये बातें लागू नहीं होतीं।
उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 9 साल की उम्र के अमरीकी बच्चों से खेल के मैदान में रखी 40 चीज़ों की जगहों को याद रखने को कहा। ये बच्चे इन चीज़ों के नामों को बार-बार दोहराकर याद रखने की कोशिश करने लगे। असंगत चीज़ों को याद रखने के लिए इस्तेमाल की गई यह स्कूली पद्धति यहाँ असफल रही। इसके विपरीत ग्वातेमाला के माया बच्चे इसी कार्य को बेहतर कर पाए। पर जब माया बच्चों को असंगत चीज़ों की सूची को याद रखने का कार्य दिया गया तो वे उतनी अच्छी तरह से यह कार्य नहीं कर पाए (रॉगॉफ एवं वैडेल)।
ये सारे निष्कर्ष हमें बताते हैं कि सभी संस्कृतियों के बच्चों को सामान्यत: एक ही तरह के कार्यों से नहीं जूझना पड़ता। संस्कृतियाँ और उनमें बसे सामाजिकता के कायदे-कानून बच्चों को सिखाने के अलग-अलग कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। इसके कारण बच्चों का संज्ञान, जो सन्दर्भ-आधारित (contextualised) होता है, विभिन्न कार्यों और सामाजिक अनुभवों से उत्पन्न होता है।
सार यह है कि समाज-सांस्कृतिक सिद्धान्त के अनुसार सोच-विचार की जिन क्षमताओं को शुरुआती और मध्य बाल्यावस्था में विकसित होने वाला माना जाता है, वे खास सन्दर्भों और सांस्कृतिक स्थितियों की उपज हैं। जितना पहले माना जाता था, उससे कहीं ज़्यादा।
Monday, 17 April 2017
Subscribe to:
Comments (Atom)